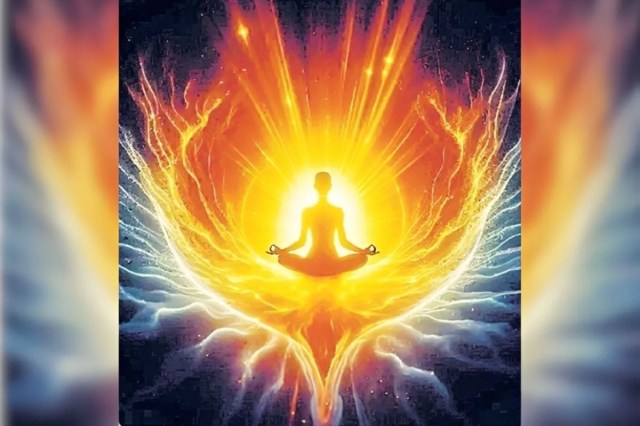प्रकाश और अंधकार साथ रहते हैं। प्रकाश का उद्गम भी अंधकार ही है। दोनों भिन्न-भिन्न संस्थाओं के कार्य क्षेत्र हैं। प्रकाश घटता-बढ़ता रहता है, अत: प्रकाश में कार्य रूप भी बदलता रहता है। प्रकाश बाधित भी हो जाता है, कार्य ठहर जाता है। प्रकाशगत संस्थाएं अंधकार में कार्य नहीं कर सकती। न ही अंधकार में जीने वाले प्राणी दिन के प्रकाश में कार्य करते हैं। जैसे कि उल्लू-चमगादड़-असुर।
हमारा शरीर ब्रह्माण्ड की प्रतिकृति है। इसमें अंधकार में भी कर्म होते रहते हैं और प्रकाश में भी। स्थूल शरीर के कर्म तो लगभग प्रकाश क्षेत्र से ही जुड़े हैं, विशेषकर आंखें। सूक्ष्म शरीर प्राण आधारित है, जिसके कार्य प्रकाश और अंधकार में समान रूप से संचालित होते हैं। आंखों के अलावा शेष चारों तन्मात्राएं अहर्निश कार्य करती हैं। प्राणों का लोक दिव्य लोक है जिसमें देव-असुर समान रूप से कार्यरत रहते हैं। इनके साथ समन्वय बिठाकर ही जीने की दिशा तय करनी पड़ती है।
सूक्ष्म शरीर के भीतर एक और शरीर है- सुसूक्ष्म शरीर या कारण शरीर। यह शुद्ध अंधकार का क्षेत्र है। अव्यय पुरुष अव्यक्त है। इसके केन्द्र में ही परात्पर कला रूप ब्रह्म की स्थिति है। जहां ब्रह्म है, वहीं माया है। माया ब्रह्म का संचालन पूर्ण अंधकार में करती है। ब्रह्म के चारों ओर माया का आवरण और गहन अंधकार बना रहता है। केवल सृष्टि पूर्व अवस्था में ही ब्रह्म मुक्त निराकार-निर्विशेष रूप रहता है।
निर्विशेष अवस्था भी प्रकाशविहीन ही है, जिसे प्रलय काल कहा जाता है। चारों ओर जल समुद्र-वरुण का साम्राज्य रहता है। चारों ओर अंधकार और आसुरी शक्तियों की गतिविधियां रहती हैं। माया वहां सुप्त रहती है। ब्रह्म निराकार है। सोम समुद्र के अधिष्ठाता स्वयं विष्णु भी निद्रा मग्न रहते हैं। प्रलय के संकेत रूप में विष्णु की नाभि में स्वयंभू ब्रह्मा की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। वही विष्णु का हृदय रूप केन्द्र है- सूक्ष्म शरीर है। ब्रह्मा की आसुरी शक्तियों से रक्षा के लिए ही निद्रा देवी का आह्वान देवता करते हैं। दुर्गा ही असुरों का संहार करती है। इसे ही विष्णुमाया कहा गया—
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:॥ (दुर्गा सप्तशती)
ब्रह्मा अव्यक्त-अव्यय है। अश्वत्थ रूप है। यही सूक्ष्म-स्थूल रूप ऊर्ध्व (क:) तथा अध: विश्व बनता है। एक अव्यक्त भाव, दूसरा व्यक्त भाव। अव्यय ही हृदय है, मन की प्रतिष्ठा का आधार है। हृद् प्रजापति को अग्नि कहा है। इसके सिर और पैर नहीं होते—
स जायत प्रथम: पस्त्यासु महो बुध्ने रजसो अस्य योनौ ।
अपादशीर्षा गुहमानो अन्तायोयुवानो वृषभस्य नीळे ॥ (ऋग्वेद 4.1.11)
यह गुह्य अग्नि वामन कहलाता है। क: प्रजापति ही केन्द्र के दोनों ओर फैलता है, रेखा और परिधि बनाता है। यही वामन का विराट् रूप है। गुह्य अग्नि (प्राण) ही यज्ञ मेें आकर तीन अग्नियों के रूप में जन्म लेता है—आह्वनीय, दक्षिणाग्नि और गार्हपत्य। यही मन, प्राण, वाक् है, अव्यय-अक्षर-क्षर है। जिस प्रकार प्रत्येक वृषा कण में ब्रह्म प्रतिष्ठित रहता है जो कि हर अस्तित्व को ब्रह्मास्मि का दर्जा देता है। उसी प्रकार हर योषा भाव के केन्द्र में माया रहती है। धरती को भी हमने मां कहा है। पंचाग्नि के सिद्धान्त का ये भी एक पड़ाव है। वर्षा की बूंदों के साथ जीवात्मा पृथ्वी के गर्भ में स्थापित हो जाता है। उसकी प्रतिष्ठा वहां जाकर होती है जहां प्रकाश नहीं पहुंच पाता। जिस प्रकार मानव स्त्री के गर्भान्त में जाकर ब्रह्म योषा में प्रविष्ट हो जाता है। यह अंधकार ही माया है। यही ब्रह्मांश के स्वरूप को पूरी तरह पहचानती है। उसकी भूमिका को उस योनि में पूरी तरह समझती है। धरती को भी पता है कि जिस औषधि में अन्न का दाना तैयार होगा, उसका कौन-कौन सा अंग किस किस प्राणी के वैश्वानर में जाएगा। उसी प्रकार वह उस औषध-शरीर के अंग-प्रत्यंगों में जीवात्मा के अंशों की प्रतिष्ठा करती है।
पृथ्वी के उस गर्भ में माया पूरी 84 लाख योनियों की योजना बना रही है। उसको यह भी पता है कि इस अन्न का दाना कौन से क्षेत्र का प्राणी खाएगा- (बिक कर कहां जाएगा)। उन परिस्थितियों को ध्यान रखकर वह ब्रह्म के अंश का विभाजन करती है। माया स्वयं अंधकार है और पृथ्वी के गर्भ में भी अंधकार है। उसमें ब्रह्म के अंश का यह विभाजन क्या ईश्वरीय चमत्कार नहीं है? क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि धरती मां यह जानती है कि उस औषधि और वनस्पति से किन-किन प्राणियों की देह का निर्माण होगा, उन प्राणियों की आयु कितनी होगी एवं उनका स्वभाव क्या होगा।
उदाहरण के लिए हम किसी फल को लें जिसे एक किसान जमीन में बोता है। एक गुठली को बोने के लिए किसान जमीन को कितना गहरा खोदता है ताकि वह गुठली सीधी धरती के मह:लोक में पहुंच जाए। इसके पूर्व भी मूल बीज पर जो आवरण चढे़ हुए हैं उनको हटाने का क्रम बनता है। अव्यय, अक्षर और क्षर तीनों ही ब्रह्म पर आवरण रूप हैं। जब तक ये आवरण नहीं हटेंगे, मूल बीज माया के सम्पर्क में नहीं आएगा। उस अंधकार में डूबना ही इस ब्रह्म की कामना है। और आगे जो जल से सिंचन होगा तब वहां अंकुरण पैदा होने लगेगा।
जिस प्रकार माता के गर्भ में शिशु आठ अवस्थाओं में पूर्ण रूप लेता है, जिस प्रकार जल आठ अवस्थाओं में पृथ्वी रूप में परिणत होता है। ठीक उसी प्रकार ये बीज भी आठ अवस्थाओं में पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होता है। पृथ्वी की धातुओं ने पेड़ के शरीर का निर्माण शुरू किया। उसके अंग-प्रत्यंग बीज में प्रतिष्ठित मानचित्र के अनुरूप उत्पन्न किए। तना-शाखा-प्रशाखा-पत्ते-पुष्प और फल पर्यन्त सम्पूर्ण देह को खड़ा किया। स्वयं प्राण रूप में इस शरीर में प्रवाहित होकर हर अंग की चिति को व्यवस्थित रखते हुए फलपर्यन्त प्रवाहमान बनी रही। फल का बीज से सम्बन्ध देह रूप में भी यहां स्पष्ट हो जाता है। जिस किस्म के आम की गुठली थी उसी किस्म के नए आम उस पेड़ को प्राप्त होते हैं। पर माया का कर्म तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उस नए फल में मूल फल का रस गन्ध आदि सभी नहीं पहुंच जाते। यह काम परा प्रकृति का है। हमारे शरीर का अंतिम धातु शुक्र है। जब तक उसमें नया आम पैदा करने की क्षमता नहीं आती तब तक न आम पूरा होता है न ही माया का कार्य पूरा होता है। परा और अपरा प्रकृति के कार्य आज के वैज्ञानिक समझने का प्रयास कर रहे हैं। काफी सीमा तक आगे भी बढ़े हैं किन्तु ब्रह्म का स्थानान्तरण बीज से लेकर फल में कैसे हो रहा है, यह शुद्ध माया के मूल कर्म का हिस्सा है। जहां किसी उपकरण की पहुंच अभी तक संभव नहीं हो पाई है।
माया अपरा और परा प्रकृति के साथ भी चलती रहती है किन्तु अभिव्यक्त नहीं होती न अलग हो सकती है। दोनों प्रकृतियों के साथ मिल कर आगे बढ़ना ही सृष्टि की पूर्णता भी होगी। सृष्टि की अभिव्यक्ति तो क्षर या अपरा प्रकृति ही है। न परा अभिव्यक्त कर पाती और न ही माया। ब्रह्म की उस कामना (एकोऽहं बहुस्याम) की पूर्ति होते हुए माया के कर्म को समझ सकते हैं।
–क्रमश: gulabkothari@epatrika.com